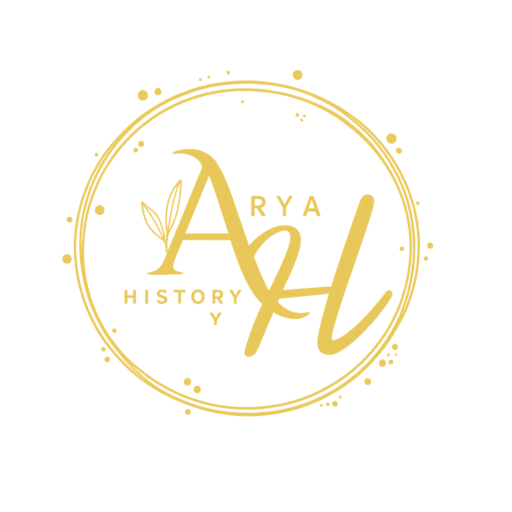नमस्कार दोस्तों, जब मैंने शंकराचार्य जी की Philosophy (अद्वैत वेदांत) पर ब्लॉग लिखा तो मैंने देखा इसके अलावा भी बहुत-सी Philosophy हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी और जरूरत भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए और exams के लिए जरूरत।
हमारे भारतीय दर्शन की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ सिर्फ पूजा-पाठ की बातें नहीं होतीं, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, सच्चाई क्या है और उसे समझने का सही तरीका कौन-सा है।
इन दर्शनों ने सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण सोच को भी जन्म दिया। हर दर्शन ने जीवन को देखने का एक नया नज़रिया दिया, कहीं तर्क का रास्ता, कहीं अनुभव का, कहीं ध्यान का और कहीं कर्म का।
तो चलिए अब हम एक-एक करके इन दर्शनों को समझते हैं और देखते हैं— कि आखिर हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हमारे जीवन के रहस्यों को किस तरह समझा था।
हमारे भारतीय दर्शनों को दो मुख्य भागों में बाँटा जाता है
- आस्तिक दर्शन (Vedic / Orthodox)
- नास्तिक दर्शन (Non-Vedic / Heterodox)
Contents
- 1 आस्तिक दर्शन (Vedic / Orthodox)
- 2 नास्तिक दर्शन (Non-Vedic / Heterodox)
- 3 अन्य / मिश्रित दर्शन – जिनके “निर्माता” या प्रवर्तक निश्चित नहीं
- 4 षड्दर्शन – आस्तिक दर्शन का विस्तार
- 5 न्याय दर्शन – तर्क से सत्य की खोज
- 6 किसने और कब शुरू किया?
- 7 Main Points —
- 8 जीवन में विवेक का उपयोग
- 9 वैशेषिक दर्शन – परमाणु और पदार्थ की समझ
- 10 किसने और कब शुरू किया?
- 11 मुख्य विचार
- 12 जीवन में उपयोग
- 13 सांख्य दर्शन – प्रकृति और पुरुष का ज्ञान
- 14 कब और किसने शुरू किया?
- 15 मूल सिद्धांत – दो शाश्वत तत्व
- 16 25 तत्वों का सिद्धांत
- 17 जीवन में महत्व
- 18 योग दर्शन (साधना से मुक्ति का रास्ता)
- 19 किसने शुरू किया और कब?
- 20 अष्टांग योग – आठ कदमों का रास्ता
- 21 योग दर्शन का असली सार
- 22 जीवन में योग दर्शन की अहमियत
- 23 पूर्व मीमांसा दर्शन(कर्ममीमांसा)– कर्म और यज्ञ का महत्व
- 24 किसने शुरू किया और कब?
- 25 मुख्य विचार
- 26 मीमांसा दर्शन का उद्देश्य
- 27 जीवन में इसका महत्व
- 28 उत्तर मीमांसा (वेदांत दर्शन) – आत्मा और ब्रह्म का एकत्व
- 29 किसने शुरू किया और कब?
- 30 मुख्य विचार
- 31 वेदांत दर्शन का उद्देश्य
- 32 Like this:
आस्तिक दर्शन (Vedic / Orthodox)
- तो भाई, जो वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं।
- इनकी कुल 6 प्रमुख प्रणालियाँ (षड्दर्शन) हैं।
- लेकिन ध्यान रहे इन 6 के भीतर भी कई उपशाखाएँ (sub-schools) हैं।
| दर्शन | प्रवर्तक | प्रमुख उपशाखाएँ / रूप |
|---|---|---|
| न्याय दर्शन | गौतम ऋषि |
नव्य-न्याय (गौड़ीय, मैथिल) जैसे गौड़ेश्वर और गंगेश उपाध्याय द्वारा विकसित, तर्कशास्त्र और प्रमाणशास्त्र की नींव। |
| वैशेषिक दर्शन | कणाद ऋषि |
परमाणु सिद्धांत वाला दर्शन; बाद में न्याय दर्शन के साथ मिला-“न्याय-वैशेषिक” परंपरा बनी। |
| सांख्य दर्शन | कपिल मुनि |
25 तत्वों का सिद्धांत; आगे चलकर योग दर्शन से जुड़ गया। |
| योग दर्शन | पतंजलि मुनि |
सांख्य पर आधारित; “अष्टांग योग” की परंपरा; उपशाखाएँ– हठयोग, राजयोग, लययोग, भक्ति योग आदि |
| पूर्व मीमांसा (कर्ममीमांसा) | जैमिनि ऋषि |
कर्मकांड प्रधान दर्शन; बाद में दो उपशाखाएँ बनीं– भट्ट मत (कुमारिल भट्ट) और प्रभाकर मत (प्रभाकराचार्य) |
| उत्तर मीमांसा (वेदांत दर्शन) | व्यास मुनि (बाद में आचार्य शंकर, रामानुज, माधव आदि ने विस्तार किया) |
कई उपशाखाएँ बनीं; • अद्वैत वेदांत – आदि शंकराचार्य; • विशिष्टाद्वैत वेदांत – रामानुजाचार्य; • द्वैत वेदांत – माधवाचार्य; • द्वैताद्वैत वेदांत – निम्बार्काचार्य; • शुद्धाद्वैत वेदांत – वल्लभाचार्य; • अचिन्त्य भेदाभेद वेदांत– चैतन्य महाप्रभु |
नास्तिक दर्शन (Non-Vedic / Heterodox)
जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते।
| दर्शन | प्रवर्तक | प्रमुख उपशाखाएँ / मत |
|---|---|---|
| चार्वाक दर्शन (लोकायत) | बृहस्पति |
– भौतिकवादी दृष्टिकोण (Materialism) – केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य मानते हैं – आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म का निषेध |
| बौद्ध दर्शन | गौतम बुद्ध |
– चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित दर्शन – प्रमुख उपशाखाएँ: • वैभाषिक • सौत्रांतिक • योगाचार • माध्यमिक |
| जैन दर्शन | महावीर स्वामी |
– अहिंसा, अपरिग्रह और सापेक्षवाद पर आधारित दर्शन – आत्मा और कर्म सिद्धांत को मानता है – दो प्रमुख शाखाएँ: • दिगंबर मत • श्वेतांबर मत |
अन्य / मिश्रित दर्शन – जिनके “निर्माता” या प्रवर्तक निश्चित नहीं
| दर्शन / परंपरा | प्रमुख व्यक्ति / प्रवर्तक | टिप्पणी |
|---|---|---|
| तंत्र दर्शन | परंपरा शिव–शक्ति उपासना से जुड़ी; विशेष रूप से “अगम” ग्रंथों से | किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, धीरे-धीरे विकसित हुआ। |
| भक्ति दर्शन | अनेक संत – जैसे रामानुजाचार्य, मीरा, तुलसी, कबीर, चैतन्य आदि | यह एक सामाजिक-आध्यात्मिक आंदोलन था, न कि एक सूत्रकार द्वारा निर्मित प्रणाली। |
| सूफी दर्शन | हज़रत अली, रूमी, बुल्ले शाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आदि | इस्लामी रहस्यवाद से प्रभावित विचारधारा, किसी एक प्रवर्तक की नहीं। |
| नव्य-न्याय दर्शन | गंगेश उपाध्याय (13वीं सदी, मिथिला) | पुराने न्याय दर्शन का तर्कवादी विस्तार। |
| आधुनिक भारतीय दर्शन | स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, गांधी, टैगोर आदि | आधुनिक युग के विचारक, जिन्होंने वेदांत व उपनिषदों की नयी व्याख्या की। |
षड्दर्शन – आस्तिक दर्शन का विस्तार
न्याय दर्शन – तर्क से सत्य की खोज
न्याय दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे पहली शाखा है। इसका मकसद है – तर्क, अनुभव और प्रमाणों के सहारे यह समझना कि असली सत्य क्या है और भ्रम क्या।
किसने और कब शुरू किया?
इस दर्शन की शुरुआत गौतम ऋषि ने लगभग 600–200 ईसा पूर्व की थी। उन्होंने बताया कि सोच-समझकर, सही तरीके से सवाल पूछकर और प्रमाणों से जवाब ढूंढकर हम सच्चाई तक पहुँच सकते हैं। कालक्रम – B.C. & A.C. को समझो
चलो अब थोड़ा गौतम ऋषि के बारे में भी जान लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म वैदिक काल में हुआ था क्योंकि इनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। इनके पिता जी का नाम रहुगण था, इनकी पत्नी अहल्या थीं। ये वही अहल्या है जिन्हें भगवान श्रीराम ने अपने पैर के अंगूठे से छू कर पत्थर से इंसान में बदल दिया था। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टी से इनका जन्म 600–500 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन रामायण 5000–6000 साल पहले और महाभारत 3000 साल पहले की घटना है।
Main Points —
- न्याय दर्शन कहता है कि कोई भी बात मानने से पहले सोचो, सवाल करो, और देखो कि उसके पीछे क्या प्रमाण है।
- यह हमें सिखाता है कि कैसे सही बात को पहचाना जाए और गलतफहमी से बचा जाए।
- बाद में गौड़ेश्वर और गंगेश उपाध्याय जैसे विद्वानों ने इसे और आगे बढ़ाया, जिसे नव्य-न्याय कहा गया। (नव-न्याय 13वीं सदी ईस्वी)
जीवन में विवेक का उपयोग
यह दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह बताता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सोच-समझकर फैसले लेना कितना ज़रूरी है।
न्याय दर्शन (Nyaya Darshan) – गौतम ऋषि का तर्कशास्त्र | 16 पदार्थों की सम्पूर्ण व्याख्या
वैशेषिक दर्शन – परमाणु और पदार्थ की समझ
तो दोस्तों, वैशेषिक दर्शन हमारे भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका मुख्य ध्यान है संसार और पदार्थ की संरचना को समझना। इसे अगर आसान शब्दों में कहें तो, यह बताता है कि हमारी दुनिया किस-किस तत्वों से मिलकर बनी है और ये तत्व कैसे आपस में जुड़े हैं।
किसने और कब शुरू किया?
वैशेषिक दर्शन की शुरुआत कणाद ऋषि ने की थी। इसका समय लगभग 600–200 ईसा पूर्व माना जाता है। कणाद ने यह बताया कि सबकुछ परमाणुओं (atoms) से बना है और हर वस्तु के पीछे नियम और कारण होता है।
मुख्य विचार
- परमाणु सिद्धांत– हर वस्तु बहुत छोटे-छोटे कणों (परमाणु) से मिलकर बनी है।
- न्याय-वैशेषिक– बाद में न्याय दर्शन के साथ मिलकर इस परंपरा को और मजबूत किया गया।
- सात मूल तत्व– पदार्थ को सात मुख्य घटकों में बाँटा गया (धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल (समय), दिशा)।
- यह दर्शन बताता है कि दुनिया में जो कुछ भी है, उसका कारण और आधार होता है।
जीवन में उपयोग
वैशेषिक दर्शन हमें तर्कपूर्ण सोच और चीज़ों के कारण समझने की आदत सिखाता है। यह केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जब हम रोज़मर्रा की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि क्यों पेड़ बढ़ते हैं, पानी क्यों बहता है तो यह दर्शन हमें सही तरीके से सोचने की आदत देता है।
वैशेषिक दर्शन– Atomic Theory Full Information
सांख्य दर्शन – प्रकृति और पुरुष का ज्ञान
चलो सुरु करते हैं सांख्य दर्शन, हमारे भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी और गहरी सोच में से एक है। इसे कपिल मुनि ने विकसित किया था, और इसका उद्देश्य है यह समझना कि हम कौन हैं, और यह संसार कैसे चलता है।
कब और किसने शुरू किया?
तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि जी माने जाते हैं। और यह दर्शन वैदिक काल के बाद, लगभग 800–500 ईसा पूर्व बीच लोगों के बीच अत्यधिक प्रिय हुआ। कपिल मुनि को “भारतीय दर्शन का वैज्ञानिक” भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जीवन और सृष्टि को समझाने के लिए तर्क और विश्लेषण(Logic and Analysis) का रास्ता अपनाया।
मूल सिद्धांत – दो शाश्वत तत्व
सांख्य दर्शन के अनुसार देखा जाए तो यह पूरा जगत दो अनादि तत्वों से बना है:-
- आत्मा (पुरुष)– चेतन, अकर्ता, निष्क्रिय और साक्षी तत्व।
- प्रकृति (प्रकृति या पदार्थ)– अचेतन, सक्रिय और सृजनशील शक्ति, जिससे पूरा ब्रह्मांड विकसित होता है।
सांख्य दर्शन – भारतीय दर्शन का वैज्ञानिक आधार
25 तत्वों का सिद्धांत
कपिल मुनि जी के अनुसार, सृष्टि की रचना 25 तत्वों से होती है —
- पुरुष (आत्मा)
- प्रकृति
- महत (बुद्धि)
- अहंकार (अहंभाव)
- मन (चित्त)
- फिर अहंकार से तीन प्रकार की सृष्टि होती है —
- सत्त्व गुण से— ज्ञानेन्द्रियाँ (कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, मन और बुद्धि)।
- रज गुण से— कर्मेन्द्रियाँ (वाणी, हाथ-पैर, जननेन्द्रिय, गुदा)।
- तम गुण से— तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध)।
- पाँच महाभूत – आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
इन सबको मिलाकर कुल 25 तत्व बनते हैं।
जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि वह प्रकृति नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा (पुरुष) है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यही सांख्य का मुख्य उद्देश्य है— ज्ञान के माध्यम से मुक्ति।
जीवन में महत्व
- यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वो प्रकृति है।
- लेकिन जो हमारे भीतर हमेशा एक-सा शांत और साक्षी बना रहता है वही आत्मा है।
- जब हम यह पहचान लेते हैं, तो दुःख और मोह अपने आप कम हो जाते हैं।
यानी सांख्य दर्शन हमें यह सिखाता है कि मुक्ति ज्ञान से मिलती है, कर्म या भक्ति से नहीं।
योग दर्शन (साधना से मुक्ति का रास्ता)
तो दोस्तों अब बात करते हैं उस दर्शन की, जो सिर्फ सोचने-समझने की बात नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाता है– योग दर्शन।
योग दर्शन हमें कहता है कि अगर मन, शरीर और आत्मा आपस में जुड़ जाएँ, तो हम खुद को समझ सकते है और मुक्ति(आज़ादी) की ओर बढ़ सकते हैं।
किसने शुरू किया और कब?
तो भाई योग दर्शन के जनक माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने करीब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच एक ग्रंथ लिखा– “योगसूत्र”।
- इसमें कुल 195 सूत्र हैं, जो योग का असली मतलब समझाते हैं।
- पतंजलि जी कहते हैं कि हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन हमरा ही अस्थिर मन है।
- मन जब शांत हो जाता है, तब इंसान अपने असली रूप ‘आत्मा’ को पहचान सकता है
अष्टांग योग – आठ कदमों का रास्ता
पतंजलि ने मोक्ष यानी मुक्ति तक पहुँचने के लिए आठ चरणों (अष्टांग) का रास्ता बताया, जिसे अष्टांग योग कहते हैं
- यम– दूसरों के प्रति सही व्यवहार (अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, लालच न करना)।
- नियम– अपने प्रति अनुशासन (साफ-सफाई, संतोष, तप, आत्म-अध्ययन, ईश्वर पर भरोसा)।
- आसन– शरीर को स्थिर और मजबूत बनाना।
- प्राणायाम– साँस को नियंत्रित करके मन को शांत करना।
- प्रत्याहार– इंद्रियों को बाहरी चीज़ों से हटाना।
- धारणा– मन को एक विचार या लक्ष्य पर टिकाना।
- ध्यान– एकाग्र होकर भीतर की ओर जाना।
- समाधि– जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाएँ, वही पूर्ण शांति की अवस्था है।
योग दर्शन का असली सार
महर्षि पतंजलि जी के अनुसार —
“योगः चित्तवृत्ति निरोधः”
मतलब, योग वह अवस्था है जहाँ मन की उथल-पुथल शांत हो जाती है।
जब मन शांत हो जाता है, तब हम अपने असली रूप को पहचानते हैं और यही मुक्ति की राह है।
जीवन में योग दर्शन की अहमियत
- तो दोस्तों, योग सिर्फ आसन या कसरत नहीं है। यह तो जीने का तरीका है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत होता है और आत्मा स्थिर।
- अगर हम रोज़ योग करें, तो हम अपने गुस्से, लालच, डर और नकारात्मक सोच पर नियंत्रण पा सकते हैं।
- और धीरे-धीरे हमारा मन इतना स्थिर हो जाता है कि हम भीतर से अपने ही मन को हल्का और शांत महसूस करते है और यही स्थिति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।
अगर सांख्य दर्शन हमें यह बताता है कि सृष्टि किन तत्वों से बनी है,
तो योग दर्शन हमें सिखाता है कि उन तत्वों से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ना कैसे है।
इसीलिए कहा जाता है–
“सांख्य और योग— सिद्धांत और साधना के दो पहलू हैं।”
पूर्व मीमांसा दर्शन(कर्ममीमांसा)– कर्म और यज्ञ का महत्व
तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस दर्शन की जो हमें काम करने के महत्व को समझाता है– पूर्व मीमांसा दर्शन।
यह दर्शन हमें बताता है कि सिर्फ ज्ञान या ध्यान से ही नहीं, बल्कि सही कर्म और यज्ञ से भी मोक्ष या मुक्ति का रास्ता बना सकते हैं।
किसने शुरू किया और कब?
तो देखो sir पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि जैमिनि। इन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व – 200 ईसा पूर्व के बीच “मीमांसा सूत्र” नामक ग्रंथ की रचना किया। ये सूत्र वेदों के कर्मकांड वाले हिस्सों को समझाने के लिए लिखे गए थे, जैसे‐ यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक कर्तव्यों को लेकर।
महर्षि जैमिनि जी मानते थे कि इंसान का धर्म है कर्म करना। कर्म के बिना सिर्फ ज्ञान या भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि कर्म ही वेदों की आत्मा है।
मुख्य विचार
पूर्व मीमांसा दर्शन का simple सिद्धांत है —
“कर्म करो, फल की चिंता मत करो।”
यह दर्शन हमें बताता है कि हर इंसान को अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे उसका फल मिले या नहीं।
- यज्ञ, पूजा, दान जैसे कर्मों से मन शुद्ध होता है।
- जब मन शुद्ध होता है, तो व्यक्ति धीरे-धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है।
मीमांसा दर्शन का उद्देश्य
तो भाई इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है — वेदों के कर्मकांड की सही व्याख्या करना और यह बताना कि कैसे यज्ञ, हवन और नित्य कर्मों के ज़रिए आत्मा की उन्नति होती है।
महर्षि जैमिनि के अनुसार —
“कर्म ही वह साधन है जिससे हम पाप से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करते हैं।”
जीवन में इसका महत्व
अगर हम इसे आसान भाषा में समझाये तो, मीमांसा दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म करते रहना ही असली साधना है। अगर हम अपने काम ईमानदारी से करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, और अपने कर्तव्य निभाते रहते हैं, तो यही “कर्मयोग” हमें मुक्ति की दिशा में ले जाता है।
पूर्व मीमांसा दर्शन हमें बताता है कि ज्ञान से पहले कर्म जरूरी है।
कर्म से मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है,
तभी आत्मा सच्चे अर्थों में मुक्ति के योग्य बनती है।
इसीलिए कहा जाता है —
“पूर्व मीमांसा धर्म का मार्ग है, और उत्तर मीमांसा मोक्ष का।”
उत्तर मीमांसा (वेदांत दर्शन) – आत्मा और ब्रह्म का एकत्व
तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे षड्दर्शन में से अंतिम दर्शन उत्तर मीमांसा दर्शन की, जिसे आमतौर पर वेदांत दर्शन कहा जाता है।
“वेदांत” का मतलब होता है वेदों का अंत। यह दर्शन हमें वेदों के सबसे गहरे बेचारों से परिचित कराता है-
- कि आत्मा (जीव) और ब्रह्म (परमात्मा) वास्तव में एक ही हैं।
किसने शुरू किया और कब?
तो दोस्तों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण (व्यासनाम) माने जाते हैं। लगभग 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच “ब्रह्मसूत्र” की रचना की थी।
- यह ग्रंथ वेदों और उपनिषदों में बताए गए सिद्धांत को तर्क के साथ समझाता है।
बादरायण जी के बाद कई महान आचार्यों ने इस दर्शन की अपनी-अपनी व्याख्याएँ दीं थी। जिनमें कुछ सबसे प्रसिद्ध हैं–
- आदि शंकराचार्य – अद्वैत वेदांत (एकत्व का सिद्धांत)
- रामानुजाचार्य – विशिष्टाद्वैत (समानता में भिन्नता)
- मध्वाचार्य – द्वैत वेदांत (ईश्वर और जीव अलग हैं)
मुख्य विचार
मैंने अद्वैत वेदांत वाले ब्लॉग में ही बताया था कि वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है — “अहं ब्रह्मास्मि”— मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब है कि जो आत्मा हमारे अंदर है,वही ब्रह्म है।
- जब हम इस सच्चाई को पहचान लेता है, तो हमारे अंदर का अज्ञान मिट जाता है और समझो हम मोक्ष पा लेते है।
- वेदांत कहता है कि अज्ञान(अविद्या) ही दुखों का कारण है। जब ज्ञान आता है, तो भेदभाव मिट जाते हैं और तब हम देखते है कि सबमें एक ही आत्मा है।
वेदांत दर्शन का उद्देश्य
तो भाई इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है- अविद्या(अज्ञान) को दूर कर ज्ञान प्राप्त करना। जब हम यह जान लेते है कि– संपूर्ण जगत उसी एक ही ब्रह्म का विस्तार है, तो उस समय हमें न कोई भय रहता है, न कोई लालच बस एक गहरी शांति मिलती है।
तो भाई यहां हर एक दर्शन का उद्देश्य एक ही है
हमें अज्ञान से निकालकर सत्य और ज्ञान की ओर ले जाना।
इन दर्शनों से हमें यही सीख मिलती है कि
जीवन में बिना सोचे-समझे किसी बात को मान लेना सही नहीं, बल्कि विचार, अनुभव, तर्क और आत्म-ज्ञान के जरिए ही सच्चाई तक पहुँचना चाहिए।
अब आप लोग हमें बताओ अगला ब्लॉग किस topic पर चाहिए??
तो दोस्तो, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आए, अगर कोई कमी लगे तो हमें comment करके जरूर बताएं अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें धन्यवाद।