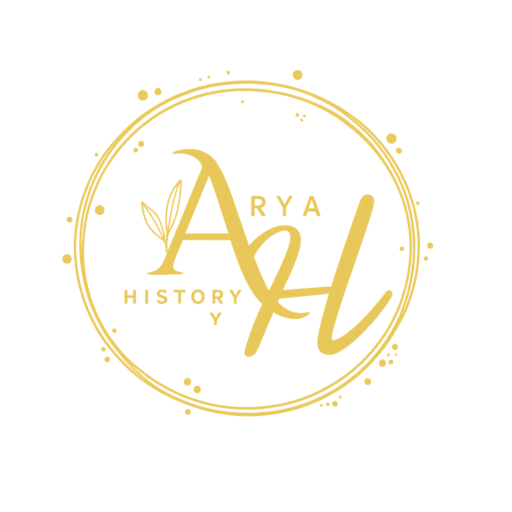प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय
हमारा इतिहास एक अत्यंत समृद्ध और विस्तृत परंपरा को समेटे हुए है, जिसमें हम सबकी प्रारंभिक सभ्यता से लेकर शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय और पतन तक की कहानी समाई हुई है। अपना इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभाजित है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं। हमारी सभ्यता का विकास लाखों वर्षों में हुआ, जिसमें हम सब ने शिकार से कृषि की तरफ, गांवों से नगरों की तरफ और जन से राज्य की तरफ लंबी यात्रा तय की है।
Contents
- 1 प्रागैतिहासिक काल (2 मिलियन ई.पू. – 1500 ई.पू.)
- 2 हड़प्पा सभ्यता / सिंधु घाटी सभ्यता (2700 – 1750 ई.पू.)
- 3 वैदिक काल (1500–600 ई.पू.)
- 4 महाजनपद काल (600 ई.पू.)
- 5 पूर्व मौर्य काल (600–321 ई.पू.)
- 6 मौर्य काल (321–185 ई.पू.)
- 7 मौर्योत्तर काल (200 ई.पू.– 300 ई.)
- 8 संगम काल (तीसरी शताब्दी ई.पू. – तीसरी शताब्दी ई.)
- 9 गुप्त काल (300–543 ई.)
- 10 वाकाटक वंश (250–500 ई.)
- 11 वर्धन/पुष्यभूति वंश(600–647 ई.)
- 12 चालुक्य वंश (543–755 ई.)
- 13 पल्लव वंश (575–903 ई.)
- 14 प्राचीन भारतीय इतिहास (निष्कर्ष)-
- 15 और ज्यादा जाने
- 16 Like this:
प्रागैतिहासिक काल (2 मिलियन ई.पू. – 1500 ई.पू.)
प्रागैतिहासिक काल वह युग है, जब हमने लेखन का विकास नहीं किया था। यह काल मुख्यतः चार चरणों में विभाजित है-
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल।
- पुरापाषाण युग (2 मिलियन ई.पू. – लगभग 10,000 ई.पू.) में मानव समाज मुख्यतः शिकार और वनस्पति एकत्र करने पर निर्भर था। इस काल में हम लोगों ने पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग किया। इस समय की गुफाएँ, जैसे कि भीमबेटका की चित्रित गुफाएँ, इस युग की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताएं मानी जाती हैं।
- मध्यपाषाण काल में हमने छोटे औजारों का प्रयोग शुरू किया और आंशिक रूप से स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे
- नवपाषाण काल (लगभग 7000 ई.पू. – 1000 ई.पू.) में कृषि का आरंभ हुआ और पशुपालन शुरू हुआ और स्थायी बस्तियाँ भी बनने लगीं। इसी काल में हमें मिट्टी के बर्तन और चमकदार पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं।
- ताम्रपाषाण काल (लगभग 3000 ई.पू. – 1500 ई.पू.) में तांबे के औजारों का प्रयोग सुरु हुआ और ग्रामीण सभ्यता का विस्तार होना सुरु हुआ।
हड़प्पा सभ्यता / सिंधु घाटी सभ्यता (2700 – 1750 ई.पू.)
हड़प्पा सभ्यता हमारी प्रथम नगरीकृत सभ्यता मानी गयी है। जिसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था और यह एक सुनियोजित नगरीय संस्कृति थी। अपने प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, और धोलावीरा शामिल हैं।
हमारी यह सभ्यता उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली , अन्नागार, मूर्तिकला, मुद्रा, लेखन प्रणाली और व्यापारिक संबंधों के लिए जानी जाती है। हमारी यह सभ्यता 1750 ई.पू. के बाद अज्ञात कारणों से पतन की ओर बढ़ने लगी।
वैदिक काल (1500–600 ई.पू.)
वैदिक काल को दो भागों में बाँटा जाता है-
- ऋग्वैदिक काल (1500–1000 ई.पू.)– इस काल में आर्य हमारे देश में आए और पंजाब व गंगा-यमुना क्षेत्र में बस गए। ये गोधन, यज्ञ, इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की पूजा, और जन आधारित समाज के लिए जाने जाते हैं।
- उत्तरवैदिक काल (1000–600 ई.पू.)– कृषि, लौह-उपयोग, जाति व्यवस्था और राज्यों की स्थापना ही हमारे इस काल की विशेषता है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जनपदों का गठन हुआ था।
महाजनपद काल (600 ई.पू.)
इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ जिनमें मगध, कोशल, अवंति, वत्स, आदि प्रमुख थे।
मगध विशेष रूप से शक्ति और विस्तार के लिए जाना गया। इसी काल में बौद्ध धर्म (महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा) और जैन धर्म (महावीर स्वामी द्वारा) की स्थापना हुई। ये धर्म हमारे समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था और यज्ञकांड की आलोचना करते हुए सरल जीवन व अहिंसा पर बल देते थे।
पूर्व मौर्य काल (600–321 ई.पू.)
इस काल में नन्द वंश का उदय हुआ, जिसने मगध को अत्यंत शक्तिशाली राज्य में बदल दिया।
इसी समय में हमारे देश पर ईरानी (फारसी) और यूनानी आक्रमण भीहुए। सिकंदर (Alexander) का अपने देश में आगमन 326 ई.पू. में हुआ, जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग तक ही सीमित रह पाया।
मौर्य काल (321–185 ई.पू.)
मौर्य साम्राज्य हमारे देश का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उनके मंत्री चाणक्य(कौटिल्य) ने अर्थशास्त्र की रचना की।
अशोक महान इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट(शासक) था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया। मौर्य प्रशासन की राजस्व प्रणाली और विदेश नीति अद्भुत मानी जाती है।
मौर्योत्तर काल (200 ई.पू.– 300 ई.)
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमारे देश में कई छोटे-छोटे राजवंशों का उदय हुआ।
●शुंग और कण्व वंश मौर्य उत्तराधिकारी थे।
● सातवाहन, चेदि, इंडो-ग्रीक, शक और कुषाण साम्राज्य उभरे।
- कुषाण वंश के कनिष्क ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया और गांधार कला का विकास किया था।
संगम काल (तीसरी शताब्दी ई.पू. – तीसरी शताब्दी ई.)
दक्षिण भारत में संगम युग तमिल साहित्य और सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल माना जाता है।
इस युग में चोल, चेर, और पाण्ड्य वंशों का सासन था। संगम साहित्य में प्रेम, युद्ध, समाज, प्रकृति आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। यह काल दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दिखाता है।
गुप्त काल (300–543 ई.)
गुप्त वंश का काल (300–543 ई.) हमारे इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता है और इसे अक्सर ‘स्वर्णिम युग’ के नाम से संबोधित किया जाता है। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) जैसे प्रसिद्ध शासकों का शासन रहा।
इस युग में कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कालिदास, आर्यभट्ट, और वराहमिहिर जैसे विद्वान इसी काल की देन हैं।
वाकाटक वंश (250–500 ई.)
वाकाटक वंश मध्य भारत में गुप्तों के समकालीन (उसी समय) थे। इसी वंश के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, जो आज भी अद्भुत कला का प्रतीक हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया।
वर्धन/पुष्यभूति वंश(600–647 ई.)
इस वंश के महान शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने उत्तर भारत को एकजुट किया। हर्ष एक विद्वान सम्राट थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उनके दरबार में बाणभट्ट जैसे विद्वान और चीन के यात्री ह्वेनसांग भी आए थे।
चालुक्य वंश (543–755 ई.)
चालुक्य वंश ने दक्कन क्षेत्र में शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था, जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था। चालुक्य काल कला और मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
पल्लव वंश (575–903 ई.)
पल्लव वंश दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य था। जिसमें महेंद्रवर्मन और नरसिंहवर्मन जैसे शासकों ने कला, वास्तुकला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। महाबलीपुरम के शिल्प उनके काल की देन हैं।
प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक काल || प्राचीन, मध्यकालीन, और आधुनिक इतिहास
प्राचीन भारतीय इतिहास (निष्कर्ष)-
हमारे देश का प्राचीन इतिहास एक जीवंत गाथा है जो न केवल शासकों और युद्धों की, बल्कि संस्कृति, धर्म, दर्शन और कला की कहानी भी कहती है। इस विशाल यात्रा में भारत ने कई उतार-चढ़ाव देखे, परंतु प्रत्येक युग ने हमारी सभ्यता को एक नई दिशा दी। यह विरासत आज भी हमारे समाज, मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता में जीवित है।
THANKYOU