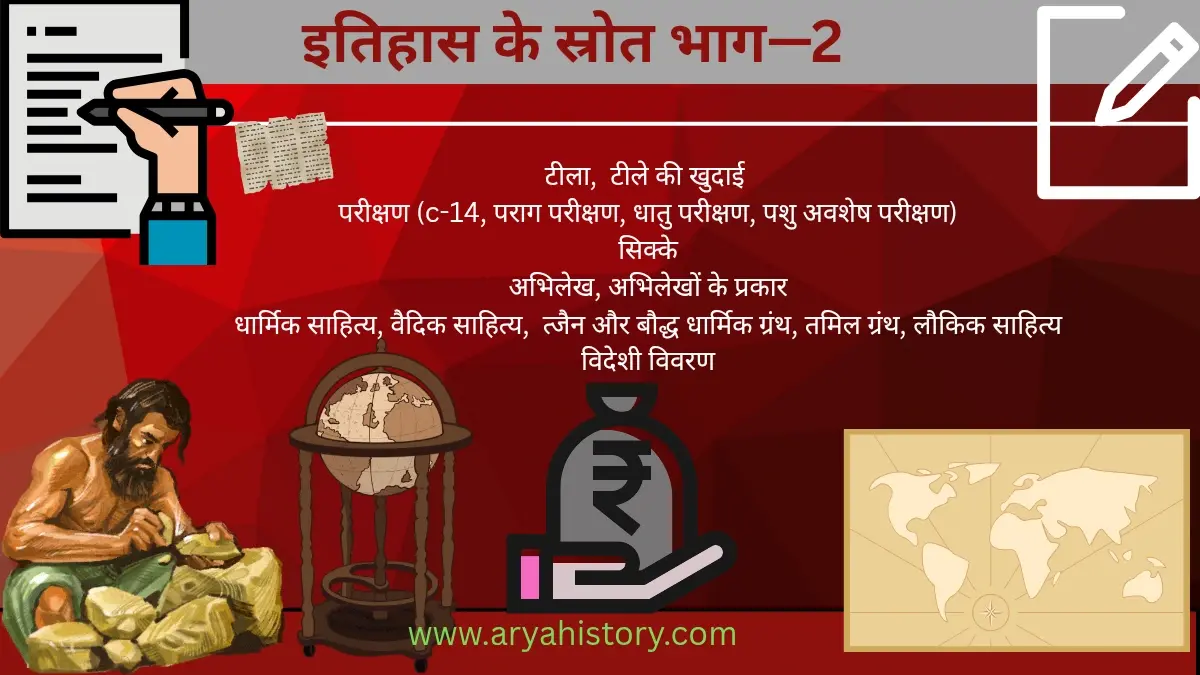🔰 इंट्रो——
पिछली बार वाले ब्लॉग (भाग 1) में ये तो क्लियर हो गया था कि इतिहास सिर्फ दादी-नानी की कहानियाँ या पौराणिक चमत्कारों का पिटारा नहीं है। असली बात तो ये है कि इतिहास जैसा कुछ है, तो वो है सबूतों के दम पर – चाहे वो किताबों में छिपा हो या ज़मीन के नीचे। हमने वहाँ पर ये भी समझा था कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत कितने ज़रूरी हैं इतिहास को समझने के लिए।
अब इस बार (भाग 2) में थोड़ा और गहराई में चलते हैं – जैसे कि टीला आखिर है क्या बला, खुदाई-फुदाई होती कैसे है, साइंटिफिक टेस्टिंग का क्या रोल है, और कैसे सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख या वेद-पुराण वगैरह हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं।
टीला किसे कहते हैं?
सीधा-सा जवाब– टीला मतलब ज़मीन का वो उभारा हिस्सा, जिसके नीचे बीते ज़माने की बस्तियाँ या सभ्यताएँ नींद ले रही होती हैं। वक्त के साथ उन पर मिट्टी, रेत, बारिश – सब जमता चला जाता है, और आखिरकार, वो ऊँचा-सा टीला दिखने लगता है। असल में, हर टीला एक टाइम मशीन है – बस खुदाई चाहिए।
टीले भी अपने-अपने टाइप के आते हैं, देख लो
1. एकल संस्कृति टीला– यहाँ पे सिर्फ एक ही संस्कृति का सामान मिलेगा, जैसे पूरी की पूरी हड़प्पा वाली सेटिंग।
2. मुख्य संस्कृति टीला– यहाँ एक मेन संस्कृति मिलती है, बाकी सब छोटे-मोटे सब-प्लॉट होते हैं।
3. बहु-संस्कृति टीला– इसमें तो मज़ा आ जाता है! ऊपर-नीचे, लेयर दर लेयर – अलग-अलग जमाने, अलग-अलग कल्चर, सब एक के ऊपर एक। महेंजोदड़ो इसका बढ़िया उदाहरण है।
टीले की खुदाई : खुदाई का खेल
टीले की खुदाई को ‘उत्खनन’ बोलते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा – फलाने गाँव में खुदाई हुई, और वहीं से कोई पुराना बर्तन, खंडहर, औजार, या कंकाल निकल आया। सच कहूँ, हर टीला एक सभ्यता का टाइमपास है – जो जितना खोदो, उतना निकलेगा।
खुदाई के भी अपने तरीके हैं-
1. अनुलंब खुदाई (Vertical Excavation)—
इसमें खुदाई सीधा ऊपर से नीचे। मकसद – अलग-अलग लेयर की कल्चरल हिस्ट्री समझना, कौन पहले आया, कौन बाद में। असली हिस्ट्री का टाइमलाइन यही सेट करता है।
2. क्षैतिज खुदाई (Horizontal Excavation)–
ये वाला तरीका एक ही समय की पूरी बस्ती, लाइफस्टाइल, घर-द्वार, सब कुछ फैलाकर समझने के लिए है। एकदम लाइफ इन एक सिंगल फ्रेम – उस जमाने का पूरा माहौल।
🔍 एक्जाम्पल? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल – इन जगहों की खुदाई दोनों स्टाइल में हुई है। पुरातत्व वाले भी क्या-क्या जुगाड़ करते हैं, है ना!
🔬 भौतिक अवशेषों की साइंटिफिक जाँच-
सिर्फ खुदाई कर ली, तो क्या? असली खेल तो शुरू होता है जब उन मिली चीज़ों की साइंटिफिक टेस्टिंग होती है। वरना, वो मिट्टी में दबे रहकर क्या ही बता पातीं!
1. रेडियो कार्बन डेटिंग (Carbon-14 Method)–
- ये वाला टेस्ट, लकड़ी या हड्डी जैसी ऑर्गैनिक चीज़ों की उम्र निकालने के लिए है।
- कार्बन-14 टाइम के साथ कम होता जाता है, तो उसकी गिनती से पता चल जाता है—कितने साल पुरानी चीज़ है।
- हड़प्पा या वेदों वाले जमाने की चीज़ों की डेटिंग ऐसे ही की गई। टाइम मशीन नहीं है, तो यही जुगाड़ है।
2. पराग परीक्षण (Pollen Analysis)-
- मिट्टी में जो छोटे-छोटे परागकण (पोल्लन) होते हैं, उनकी पड़ताल करके पता चलता है, उस एरिया में कैसी जलवायु, कैसी घास-फूस या पेड़-पौधे थे।
- इससे आप जान सकते हो कि लोग क्या खाते थे, या उस ज़माने में मौसम कैसा था। खेती-बाड़ी की भी कुछ झलक मिल जाती है।
3. धातु परीक्षण–
- जो भी ताम्बा-लोहे की चीज़ें मिलें, उनकी बनावट, क्या-क्या मिलाया गया था, कैसे बनाई गई—सबका एनालिसिस होता है।
- इससे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, या कौन-कौन सी जगहों से व्यापार होता था, इन सबका आईडिया मिलता है।
4. पशु अवशेष परीक्षण–
- खुदाई में निकली हड्डियाँ, दाँत—इनकी जाँच कर के पता चलता है, कौन से जानवर पालतू थे, कौन-से खाए जाते थे, किस पर सवारी करते थे।
- सच बोलूँ तो, इन हड्डियों से पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने जुगाड़ू थे—जो चीज़ हाथ लगी, उसका काम निकाल लिया!
चलो, सिक्कों से शुरू करते हैं—
प्राचीन भारतीय सिक्के full information
सिक्कों की पढ़ाई को ‘मुद्राशास्त्र’ बोलते हैं, अंग्रेजी वाले इसे ‘न्यूमिस्मेटिक्स’ कहते हैं, थोड़ा फैंसी सा नाम है न? खैर, पुराने टाइम में इंडिया में सिक्के तगड़े चलते थे—तांबा, चांदी, सोना, सीसा, सबका इस्तेमाल हुआ, और मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे भी इतने सारे मिले कि गिनती मुश्किल है, खासतौर पर कुषाण से गुप्तोत्तर काल तक।
शुरुआत में सिक्कों पे बस कुछ सिंबल्स मिलते हैं, लेकिन आगे चलकर तो राजा, देवता, तारीख—सब कुछ छाप दिया। असल में, कई डाइनास्टियों का इतिहास ही इन सिक्कों की वजह से दोबारा लिख डाला गया, हिन्द-यवन शासकों के बारे में तो बहुत कुछ इन्हीं से पता चला। और हां, सिक्के सिर्फ देखने के लिए नहीं थे—दान, खरीदारी, वेतन-मजदूरी, सब कुछ इन्हीं से चलता था। इससे उस टाइम की इकोनॉमी पर भी काफी रोशनी पड़ती है।
ट्रेडर्स और ज्वेलर्स की अपनी-अपनी गिल्ड चलती थी, जाहिर है, उस समय की शिल्पकला और कारोबार मस्त लेवल पर था। सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य के बाद के टाइम में मिले, फिर गुप्तोत्तर काल आते-आते सिक्कों की गिनती घट गई—मतलब, ट्रेड-ट्रांजैक्शन भी सुस्त पड़ गए होंगे। और हां, देवताओं की फोटो, धार्मिक निशान, और तरह-तरह की इबारतें भी सिक्कों पर मिलती हैं, जिससे उस जमाने की आर्ट और फेथ का आइडिया मिलता है।
अब आते हैं अभिलेखों पे—
इनकी चेकिंग को पुरालेखशास्त्र (एपिग्राफी) बोलते हैं। ये अभिलेख तो जगह-जगह मिलते हैं—मुद्राओं, पत्थर के खंभों, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवारें, ईंटें, मूर्तियां… मतलब, जहां जगह मिली, वहां खुदवा दिया। स्टार्टिंग में तो पत्थर पर ही मिलते हैं, लेकिन ईसा की शुरुआती सदियों में ताम्रपत्र आ गए। साउथ इंडिया में तो मंदिरों की दीवारें अभिलेखों से पट गई हैं।
शुरू के अभिलेख प्राकृत में (तीसरी सदी ई.पू.), बाद में संस्कृत छा गई—चौथी-पांचवी सदी तक तो हर जगह संस्कृत ही दिखती है। मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तकाल के ज्यादातर अभिलेख ‘कार्पस इन्सक्रिप्शनम इंडिकेरम’ नाम की मोटी किताब में मिलते हैं, लेकिन गुप्तोत्तर और साउथ के 50,000+ अभिलेख अभी भी कबाड़खाने में पड़े हैं, कोई इनका इंतजार कर रहा है कि कब छपेंगे!
हड़प्पा वालों की लिपि अब तक डिकोड नहीं हुई, उदास खबर है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक में मिले—इनको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, भाई ने कमाल कर दिया था।
अभिलेखों के टाइप्स की बात करें—
- कुछ में सरकारी फरमान, पब्लिक के लिए सूचना वगैरह।
- दूसरी कैटेगरी में रिचुअल वाले—बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव—सबने अपने मंदिर, मूर्तियों पर खुदवाए।
- तीसरे टाइप में प्रशस्तियाँ यानी राजाओं की तारीफ—“मैंने ये किया, मैंने वो किया”—पूरा सेल्फ-प्रमोशन! और हां, दानपात्र भी मिले जिनमें पैसा, जानवर, ज़मीन दान देने की डीटेल्स हैं।
- भूदान अभिलेखों से उस टाइम की ज़मीन और एडमिन सिस्टम का भी पता चलता है।
अब थोड़ा साहित्यिक सोर्सेज़ पर चलते हैं—
लोगों को लिपि का आईडिया तो 2500 ई.पू. से था, लेकिन सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ चौथी सदी ईस्वी से पहले की नहीं मिलती। प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, सब कुछ भोजपत्र-तालपत्र पे हाथ से लिखा जाता था।
धार्मिक साहित्य—
ज्यादातर पुराने ग्रंथ तो धर्म से ही जुड़े हैं। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन-बौद्ध ग्रंथ—इन सब से हमें इंडिया की सोसाइटी और कल्चर की झलक मिलती है।
वैदिक लिटरेचर की बात करें तो—
ऋग्वेद (1500-1000 ई.पू.), बाकियों (अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद) को 1000-500 ई.पू. का माना जाता है। ऋग्वेद में देवताओं की तारीफें, बाद के लिटरेचर में पूजा-पाठ, जादू-टोना, पौराणिक कहानियां। उपनिषदों में फिलॉसफी वाला टच है। महाभारत, रामायण, पुराणों का फाइनल एडिशन करीब 400 ई. के आसपास हुआ।
इसके बाद कर्मकांड लिटरेचर की बाढ़—
श्रौतसूत्र (पब्लिक यज्ञ, राज्याभिषेक की रस्में), गृहसूत्र (जन्म, नामकरण, उपनयन, शादी, श्राद्ध—घर के सारे फंक्शन), शुल्बसूत्र (यज्ञवेदी के नाप-जोख के नियम)।
अब जैन-बौद्ध ग्रंथ—
इनमें असली-नकली, सब ऐतिहासिक बंदों और घटनाओं की डीटेल्स मिलती हैं। सबसे पुराने बौद्ध ग्रंथ पालि में थे, ई.पू. दूसरी सदी में श्रीलंका में फाइनल कंपाइल हुए। इनमें बुद्ध के पुराने जन्म, पांचवीं सदी ई.पू. से दूसरी सदी ईस्वी तक की सोशियो-इकॉनॉमिक कंडीशन दिखती है।
जैन ग्रंथ प्राकृत में, छठी सदी ईस्वी में वल्लभी (गुजरात) में फाइनल हुए। जैन ग्रंथों से बिहार-पूर्वी यूपी की पॉलिटिक्स और व्यापारियों के बारे में पता चलता है।
लौकिक साहित्य में—
1.विधि ग्रंथ—धर्मसूत्र (500-200 ई.पू.), स्मृतियाँ (पहली छह सदी),
2.टीकाएँ—इन सबको मिलाकर धर्मशास्त्र कहते हैं। इनमें वर्ण, राजा, अफसर, संपत्ति, बिक्री, वारिसी, सजा—सब कुछ लिखा है।
3.कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’ तो मास्टरपीस है—मौर्यकाल का पूरा सिस्टम दिखता है।
4.भास, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट—इनकी रचनाओं में अपने-अपने टाइम का पूरा माहौल झलकता है।
तमिल ग्रंथ—
ओह भाई, ये तो संगम साहित्य में आते हैं। सोचो, राजाओं के टाइम में कवि और भाट सब विद्या केंद्रों में बैठे, चाय-वाय पीते हुए (ठीक है, शायद चाय नहीं), तीन-चार सदियों तक इकट्ठा करते रहे ये रचनाएँ। ये ग्रंथ ईसा की शुरुआत से लेकर छठी सदी तक धीरे-धीरे तैयार हुए—कोई एक रात की बात नहीं थी।
अब संगम ग्रंथों को वैदिक ग्रंथों से मत मिला देना। ये कोई धर्म-शास्त्र नहीं हैं। ये तो असली, ज़िंदगी की बातें हैं—हीरो-हीरोइन की तारीफ, शहरों का हाल, यवनों से व्यापार, तमिलनाडु का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक किस्सा—सब कुछ मिल जाएगा। नाम सुनो—कवरीपट्टनम! कितना कूल लगता है न?
अब आते हैं विदेशी लोगों की बात पर-
देखो, देसी साहित्य को जबरदस्ती अकेला न छोड़ो, उसमें विदेशी यात्रियों की बातें भी डालो, मजा ही आ जाएगा।
यूनानी, रोमन, चीनी—सबने इंडिया का टूर किया, अपनी डायरी में नोट्स भी बनाए।
सिकंदर के हमले की न्यूज भी उन्हीं ग्रीक सोर्सेस से मिलती है। वहां एक सॅन्ड्रोकोटस नाम लिखा मिला, बाद में पता चला कि यही अपना चंद्रगुप्त मौर्य है। इसने तो इतिहास की नींव ही बदल दी।
अब मेगस्थनीज की इंडिका—
1. यार, इससे मौर्य राज, वहां के लोग, उनकी लाइफस्टाइल सब पता चलता है।
2. ग्रीक में लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, 80 से 115 ई. के बीच का—इसमें पूरा समुद्री व्यापार का लेखा-जोखा है।
3. टॉलेमी की जियोग्राफी (150 ई.) भी कमाल है, प्राचीन नक्शे, ट्रेड रूट—सबकुछ!
प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका?
भारत-इटली के व्यापार की डीटेल्स उसमें हैं। और, चीनी पर्यटक? फा-हियान और हुआन सांग—दोनों बौद्ध थे, दोनों ने इंडिया की सैर की।
फा-हियान ने गुप्त काल वाली इंडिया की लाइफ बताई, तो हुआन सांग ने हर्ष के टाइम की। कुल मिलाकर, देसी-विदेशी सब मिल जाएं, तभी असली तस्वीर बनती है।
इतिहास पढ़ना मतलब बस किताबें रटना नहीं, यार। असली मजा तो तब है जब उन सब चीज़ों की खोज में निकलो, जो हमारे पुरखों ने जाने-अनजाने छोड़ दीं — कभी मिट्टी में दबा दीं, कभी पत्थर पर उकेर दीं, कभी किसी ताम्रपत्र पर लिख दीं, और हां, कभी-कभी तो विदेशी घूमन्तुओं की डायरी में भी मिल जाती हैं।
देखो, पुरातात्विक चीजें? सीधा जमीन से मिलती हैं, असली-खालिस सबूत।
सिक्के, शिलालेख? राजा-महाराजाओं की कहानियों के साथ धर्म की झलक भी दिखा देते हैं।
ताम्रपत्र-साहित्य? समाज, रीति-रिवाज, सब कुछ खोल के रख देते हैं।
विदेशी मुसाफिरों की बातें? भाई, वो तो जैसे बाहर से आई CCTV फुटेज है — बिल्कुल अलग नजरिया।
इतिहास कोई फैंटेसी सीरीज़ नहीं, सब कुछ ठोस सुबूतों पर टिका है। और आज के टाइम में, खासकर UPSC वालों — सुन रहे हो न? — तुम्हारे लिए ये सब जानना, समझना जरूरी है। वरना एग्जाम में क्या ही कर पाओगे!
✍️ और जाते-जाते एक छोटी सी शायरी….
स्रोतों की ये बातें, इतिहास की असली जान,
हर टुकड़ा बोलता है, बीते कल का बयान।
कभी पत्थर पे लिखा, कभी ताम्रपत्र में दर्ज,
हर निशानी, हर लफ्ज़, अतीत को कर दे गर्व।