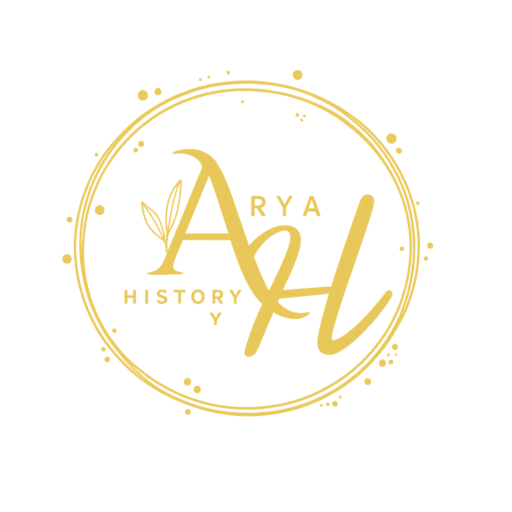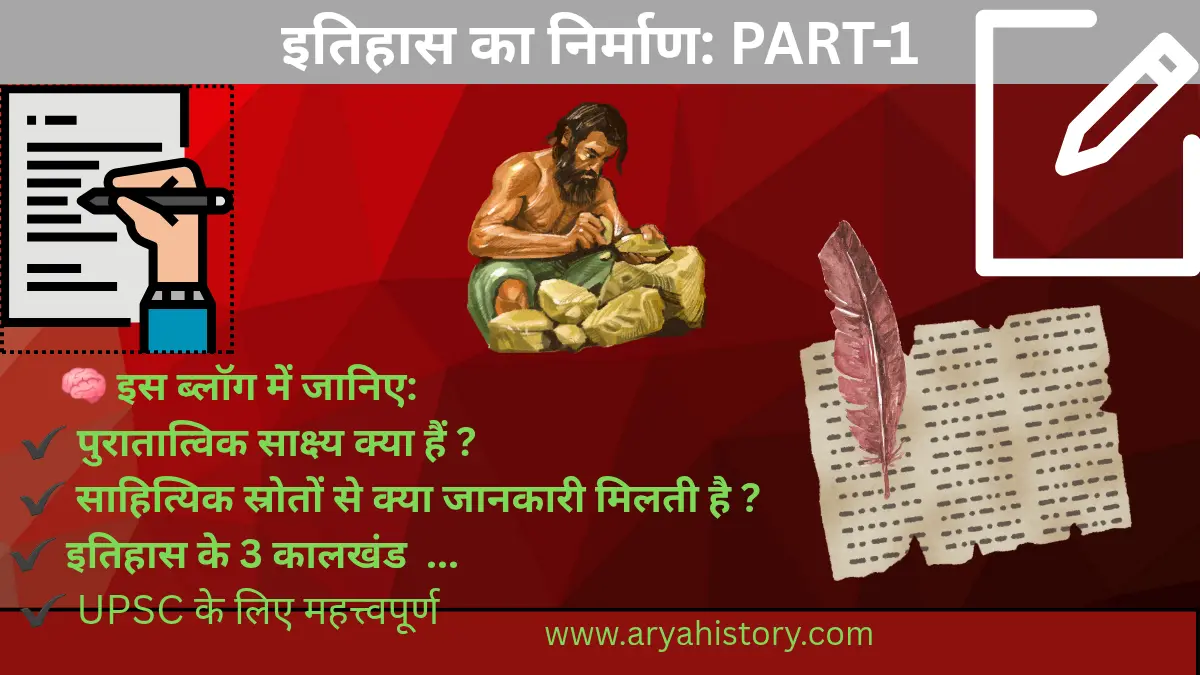Contents
- 1 कभी आपने सोचा है कि हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिली कैसे? आज जो कुछ भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हमें कैसे मिली? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल आदि की जानकारी हमारे इतिहासकारों को कैसे मिली? ये सब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि जब हम अपने अतीत को जानते हैं, तभी हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं।
- 2 स्रोतों के प्रकार- इतिहास जानने के दो प्रमुख आधार
- 3 1. पुरातात्विक साक्ष्य – मिट्टी में दबी हुई कहानियाँ
- 4 2. साहित्यिक साक्ष्य – जब शब्द बोलने लगे इतिहास
- 5 इतिहास के स्रोत (लेखन और उसके तीन कालखंड)-
- 6 1. प्रागैतिहासिक काल
- 7 2. आद्य ऐतिहासिक काल
- 8 3. ऐतिहासिक काल
- 9 हम कैसे समझें ?
- 10 Like this:
कभी आपने सोचा है कि हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिली कैसे? आज जो कुछ भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हमें कैसे मिली? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल आदि की जानकारी हमारे इतिहासकारों को कैसे मिली? ये सब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि जब हम अपने अतीत को जानते हैं, तभी हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं।
आज के समय में तो हम अपने इतिहास को दस्तावेजों के रूप में, किताबों में, डिजिटल फॉर्म में या हार्ड-कॉपी के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन पहले के समय में जब हम आदिमानव थे, जब हमें लिखना-पढ़ना भी नहीं आता था, तब भी हमारे इतिहासकारों को उस समय की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, और आज के इस ब्लॉग में हम इसी महत्त्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
स्रोतों के प्रकार- इतिहास जानने के दो प्रमुख आधार
हमारे इतिहास को जानने और समझने के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, और इन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने बीते समय की झलक हम तक पहुंचाई है। ये दोनों स्रोत हैं–
- पुरातात्विक साक्ष्य
- साहित्यिक साक्ष्य
1. पुरातात्विक साक्ष्य – मिट्टी में दबी हुई कहानियाँ
पुरातात्विक साक्ष्य यानी ऐसे सभी प्रमाण जो हमें खुदाई में प्राप्त होते हैं – वो चाहे किसी टूटे हुए बर्तन के टुकड़े हों, कोई पुरानी ईंट हो, कोई सिक्का हो, औजार हों, या फिर मूर्तियाँ। ये सब हमारे अतीत के मौन लेकिन बहुत गहरे गवाह होते हैं। जब भी हम किसी जगह खुदाई करते हैं, तो जमीन के नीचे छुपे हुए यह अवशेष हमको उस समय की कहानी सुनाने लगते हैं।
हम सबने कभी ना कभी टीवी पर या अखबारों में पढ़ा होगा कि “फलां जगह खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले” या “खुदाई में गुप्तकालीन सिक्के मिले” — तो यही सब पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं।
इन साक्ष्यों की मदद से हमारे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि उस समय के लोगों की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, उनका रहन-सहन, उनका धर्म, शासन प्रणाली कैसी थी — यह सब केवल इन वस्तुओं के आधार पर समझा गया।
हमारे लिए यह सोचने वाली बात है कि बिना कोई लिखित जानकारी के, केवल अवशेषों को देखकर कोई कैसे बता सकता है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? लेकिन हमारे पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने ये कर दिखाया है।
उदाहरण के तौर पर – हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन, ईंटें, नालियाँ, मूर्तियाँ और वजन मापने वाले उपकरण मिले हैं, उनसे हमको समझ आया कि वहां के लोग साफ-सफाई पसंद थे, व्यापार करते थे और एक संगठित समाज में रहते थे।
2. साहित्यिक साक्ष्य – जब शब्द बोलने लगे इतिहास
जैसे-जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, वैसे-वैसे हमें लिखना-पढ़ना भी आ गया। जब लोग अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखने लगे, तब से लेकर अब तक हमारे पास एक से बढ़कर एक साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं।
आपने वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों के बारे में सुना होगा — ये सब हमारे प्राचीन इतिहास का हिस्सा हैं और साहित्यिक साक्ष्य कहलाते हैं। इन ग्रंथों में उस समय की राजनीति, धर्म, समाज, जीवनशैली, शिक्षा व्यवस्था आदि की बहुत सारी जानकारी मिलती है।
इतिहासकारों ने जब इन ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्होंने यह देखा कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं, वो उस समय के समाज की झलक देती हैं। जैसे यदि किसी ग्रंथ में यह लिखा गया है कि किसी राजा ने दान में 100 गायें दीं, तो इससे हमको उस काल की आर्थिक स्थिति और सामाजिक परंपराओं का पता चलता है।
लेकिन एक बात और — जब भी हम साहित्यिक साक्ष्यों की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना होता है। क्योंकि ये साक्ष्य किसी न किसी लेखक ने अपनी दृष्टिकोण से लिखे होते हैं, और उनकी सोच, उनकी मान्यताएं, उनका झुकाव किसी खास व्यक्ति, धर्म या विचारधारा की तरफ हो सकता है।
इसीलिए इतिहासकार जब भी किसी साहित्यिक साक्ष्य का उपयोग करते हैं, तो वे कोशिश करते हैं कि उस लिखी हुई बात की पुष्टि किसी पुरातात्विक साक्ष्य से भी हो जाए। जब दोनों साक्ष्य एक-दूसरे से मेल खाते हैं, तभी उस बात को पूरी तरह प्रमाण माना जाता है।
इतिहास के स्रोत (लेखन और उसके तीन कालखंड)-
अब अगर हम प्राचीन इतिहास को समझना चाहें, तो हमें यह जानना जरूरी है कि इतिहासकारों ने प्राचीन काल को तीन भागों में विभाजित किया है। कैसे विभाजन किया और क्यूँ और इस विभाजन का आधार भी यही दो साक्ष्य — पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य ही हैं।
1. प्रागैतिहासिक काल
यह वह समय था जब इंसान को लिखना-पढ़ना नहीं आता था। हम आदिमानव के रूप में जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, आग जलाना सीख रहे थे और गुच्छों में जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं — जैसे औजार, गुफा चित्र आदि।
2. आद्य ऐतिहासिक काल
इस काल में लोग धीरे-धीरे लिखना-पढ़ना सीखने लगे थे, लेकिन अब भी हमारे पास अधिकतर प्रमाण पुरातात्विक ही हैं और बहुत सीमित साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए — हड़प्पा सभ्यता।
3. ऐतिहासिक काल
यह वह काल है जब हमारे पास पर्याप्त लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल — ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इस समय में हमें साहित्यिक और पुरातात्विक, दोनों प्रकार के साक्ष्य भरपूर मिलते हैं।
अगर आप पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं कि कौन कौन से स्रोतों का उपयोग कैसे होता है तो आप part- 2 पढ़ सकते हैं।
हम कैसे समझें ?
अब जब आप यह ब्लॉग पढ़ चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हमारे इतिहास की जानकारी सिर्फ किताबों से नहीं आई है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए इतिहास के स्रोत (चिन्हों, अवशेषों और शब्दों) का नतीजा है।
हमारे इतिहासकारों ने दिन-रात मेहनत करके, खुदाई की, प्राचीन लिपियों को पढ़ा, तुलना की, विश्लेषण किया और तब जाकर हमें एक समृद्ध इतिहास दिया है।
हम सभी को चाहिए कि हम अपने इतिहास को समझें, सराहें और इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। आप, हम, हम सब मिलकर इस विरासत को जिंदा रख सकते हैं।
अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें धन्यवाद।
अतीत की राख में छिपे थे उजाले के सूत्र,
हर साक्ष्य में बसी है भविष्य की दृष्टि।
इतिहास वही समझेगा जो प्रश्न पूछेगा,
और उत्तर वही पाएगा जो शोध करेगा।